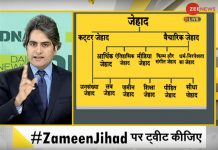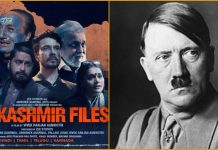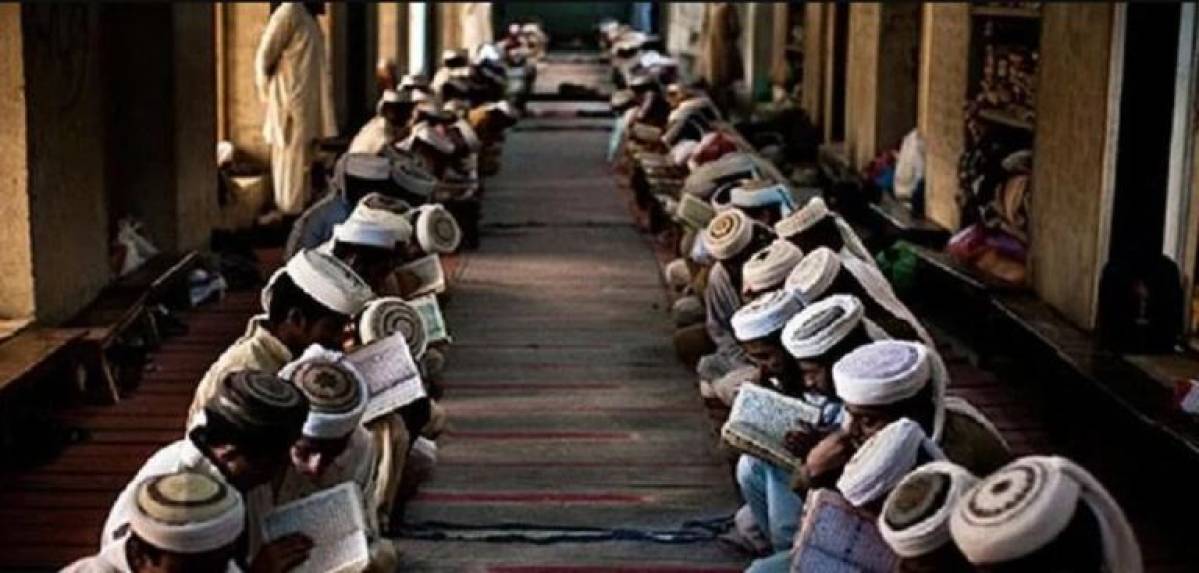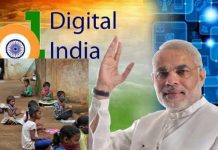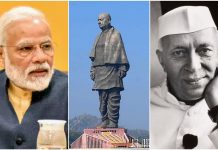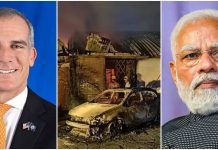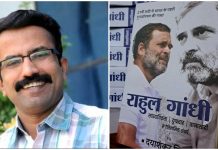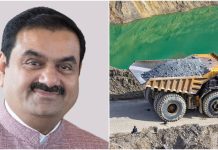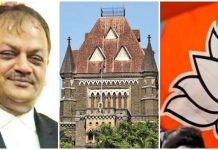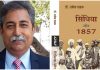गंगा सहाय मीणा
5 मार्च को बहुजन संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है. आइए, इसकी पृष्ठभूमि और कारणों को समझते हैं.
भारतीय लोकतंत्र अपनी इंद्रधनुषी छवि के कारण दुनिया का अनोखा और खूबसूरत लोकतंत्र है. सत्ता प्रतिष्ठानों में विभिन्न तबकों की हिस्सेदारी इस लोकतंत्र की आत्मा है. इस हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने हेतु संविधान में प्रावधान किये गए हैं. इस तरह की संवैधानिक व्यवस्था दुनिया के कई देशों में है जिसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से वंचित तबकों की लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाती है. भारत की आरक्षण व्यवस्था अपने लक्ष्य समावेशी लोकतंत्र को पाने की दिशा में लगातार अग्रसर है.
शिक्षा सामाजिक बदलाव का सशक्त माध्यम है इसलिए सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में वंचित तबकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्रावधान किये गए, जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश योग्यता में रियायत, विभिन्न स्कॉलरशिप और फैलोशिप, विभिन्न श्रेणियों के लिए संविधानसम्मत सीटें आरक्षित करना आदि. इसी क्रम में अन्य क्षेत्रों की तरह शैक्षिक क्षेत्र की सरकारी नौकरियों में सभी श्रेणियों को अवसर देने के लिए आरक्षण के प्रावधान किये गए हैं. इनमें भी उच्च शिक्षा का क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. यह सामाजिक न्याय की नीति के तहत किये गए संवैधानिक प्रावधानों का ही प्रतिफल है कि देश के तमाम विश्वविद्यालयों में वंचित तबकों के विद्यार्थियों के अलावा शिक्षक भी दिखाई देने लगे हैं. ये शिक्षक अपनी मेहनत और लगन से अपने विश्वविद्यालयों में विशिष्ट स्थान बना रहे हैं.
सामाजिक न्याय पर हाल ही में तीन बड़े हमले हुए हैं- पहला, उच्चतम न्यायालय का केन्द्र सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन और उसके बाद रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले को यथावत रखना, जिसके तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के रोस्टर को विभागवार लागू होगा. दूसरा, बिना किसी अध्ययन और बिना पर्याप्त बहस के आनन-फानन में सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देना. और तीसरा, लाखों आदिवासियों की बेदखली का फरमान. सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा आदेश के लागू होते ही 200 पॉइंट रोस्टर की जगह 13 पॉइंट विभागवार रोस्टर लागू हो जाएगा. साथ ही इसके अनुसार विभाग में भी आरक्षण कैडर (असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोशिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर) आधारित होगा. यानी पहली बात तो यह कि अब संस्था को एक इकाई मानने के बजाय विभाग को इकाई माना जाएगा और उसमें भी संबंधित कैडर में जब किसी श्रेणी की बारी आएगी, तभी उसके लिए एक पोस्ट आरक्षित हो पाएगी।
विभाग को इकाई मानकर 13 पॉइंट रोस्टर लागू करना आरक्षण व्यवस्था की हत्या जैसा है। इसको इस प्रकार समझिए- कल्पना कीजिए कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के कुल 200 पद हैं। संविधान प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था के अनुसार उनमें से 56 पद (27%) ओबीसी के लिए, 30 पद (15%) अनुसूचित जाति के लिए और 15 पद (7.5%) अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होने चाहिए। अभी तक जारी रोस्टर (200 पॉइंट) पद्धति के अनुसार ऊपर दी गई संख्या के आसपास सीटें विभिन्न श्रेणियों की बन जाती थी। संबंधित कॉलेज/विश्वविद्यालय भले ही बहाने बनाकर उन्हें पूरा नहीं भरते थे, लेकिन सीटें तो उतनी ही बनती थी।
अब नई पद्धति के अनुसार विभागवार रोस्टर होगा। यानी विभाग को एक यूनिट मानकर कैडर आधारित संबंधित श्रेणी के आरक्षण में प्रतिशतानुसार देर सवेर सीट बनेगी। कॉलेज या विश्वविद्यालय में भले ही कुल पद 200 हो, विभागवार अगर 4 या 5 या 6 सीटें ही अनुमोदित हैं और उनमें भी मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 सीटें हैं, एसोशिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की 1-1 सीटें हैं तो एसोशिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर कैडर में 1-1 सीट होने के कारण कभी कोई आरक्षित सीट नहीं बन पाएगी. असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पहली बार की नियुक्तियों में अजा, अजजा और ओबीसी को किसी विभाग में कोई सीट नहीं मिलेगी। 3 असिस्टेंट प्रोफेसरों में से किसी एक के रिटायर होने पर ओबीसी को एक सीट मिलेगी. अजा को 6 अध्यापकों के रिटायर होने के बाद पहली सीट मिलेगी और अजजा को 13 अध्यापकों के रिटायर होने के बाद पहली। यानी इस पद्धति में सभी आरक्षित श्रेणियों का उचित प्रतिनिधित्व रेगिस्तान के सागर की तरह ही रहेगा।
जिन आदिवासियों ने जंगलों को बचाया आज जंगल बचाने के नाम पर उन्हें ही उजाड़ा जा रहा है
सबसे ज्यादा खामियाजा अजजा (ST) को उठाना पड़ेगा। जिन विभागों में तीनों कैडर में एक-एक, यानी कुल 3 ही पद अनुमोदित हैं, उनमें किसी सीट पर कभी कोई आरक्षण नहीं हो पाएगा। अगर ज्यादा पद अनुमोदित हुए भी तो आरक्षित श्रेणियों को उचित प्रतिनिधित्व कभी नहीं हो पाएगा. अनुसूचित जाति की सीट बनते-बनते तो मुमकिन है पूरी एक सदी लग जाए. तब तक कोई नई पद्धति आ जाएगी और इस तरह नए आदेशानुसार प्रकारांतर से उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण-व्यवस्था पूरी तरह निष्प्रभावी हो जाएगी. एक तो अभी तक हजारों आरक्षित सीटों को वर्षों से भरा नहीं गया है, ऊपर से यह आदेश! उल्लेखनीय है कि सरकार की रिव्यू पिटीशन खारिज होते ही विश्वविद्यालयों में इस नए निजाम यानी विभागवार रोस्टर के अनुसार विज्ञापनों की बाढ सी आ गई. ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा तंत्र सामाजिक न्याय के विरोध में खड़ा है.
विश्वविद्यालयों को सरकार विभागवार अनुदान नहीं देती, इसलिए विभागवार रोस्टर अतार्किक है. यूजीसी का ही एक पुराना आदेश (2006 के आदेश का 6-C) पूरे विश्वविद्यालय या कॉलेज की पोस्टों की ग्रुपिंग की वकालत करता है, जबकि मौजूदा उसका विरोधी प्रतीत होता है.
यही वजह है कि देशभर के विश्वविद्यालयों में शिक्षक आंदोलित हैं. इसकी शुरूआत 5 मार्च 2018 से हो गई थी जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देकर यूजीसी ने विभागवार नियुक्तियों का एक आदेश निकाला था. बाद में यूजीसी ने तमाम नियुक्तियों की प्रक्रिया रोक दी और सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया गया. बीच में दलित-आदिवासी-पिछड़े वर्गों के सांसदों के दबाव में सरकार ने इस मसले पर एक अध्यादेश भी ड्राफ्ट किया लेकिन किसके कहने पर वह ड्राफ्ट कहां गायब कर दिया गया, कोई नहीं जानता.
चूंकि इस संदर्भ में पहला आदेश ठीक एक साल पहले 5 मार्च 2018 को आया, इसलिए बहुजन संगठनों ने इस 5 मार्च को भारत बंद करने का फैसला किया है. इस भारत बंद में लाखों आदिवासियों की बेदखली का सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी एक अहम मुद्दा है. भले ही यह बेदखली दो-तीन महीने के लिए स्थगित कर दी गई हो, लेकिन बेदखली का खतरा तो बना ही हुआ है. एक तो आदिवासियों के पक्ष में ठीक से कानून नहीं बने, और जो बने, उन्हें ठीक से लागू नहीं किया गया. मसलन 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची, ‘जनजातीय सलाहकार परिषद’ आदि बातें कागजों तक रह गईं. जंगलों पर आदिवासियों के परंपरागत अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए यूपीए सरकार ने वन अधिकार अधिनियम बनाया.
इसमें आदिवासियों और वनों के परंपरागत निवासियों के जंगलों संबंधी व्यक्तिगत और सामुदायिक हकों, जैसे- निवास व जीविका के लिए वन का उपयोग, वनोपज चुनना, चारागाह व तालाब आदि का उपयोग, पुनर्वास का अधिकार आदि को लेकर प्रावधान किये गए और बाहरी प्रशासन के बजाय स्थानीय ग्राम-सभा आदि संस्थाओं को मजबूत किया गया. जाहिर है जंगलों स्थित प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करने वाले कॉर्पोरेट को आदिवासियों व वनों के परंपरागत निवासियों को उनके अधिकार वापस किये जाना पचा नहीं, इसलिए अधिनियम आने के बाद से ही इसके ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिये. इसी प्रक्रिया में इस अधिनियम को कानूनी चुनौती भी दे दी गई.
यह अजीब बात है कि उच्चतम न्यायालय और बाद की केन्द्र व राज्य सरकारों को वन अधिकार अधिनियम को लागू करवाने हेतु प्रयत्न करने चाहिए थे लेकिन हुआ ठीक इसके उलट. राज्य सरकारों और उनके अधीन काम करने वाले अधिकारियों ने आदिवासियों व वनों के पारंपरिक निवासियों को ठीक से चीजें समझाए बिना जंगलों पर उनके दावों को खारिज कर दिया. ग्राम सभाओं की सिफारिशों को उच्च प्रशासन द्वारा बदल दिया गया. जिन आदिवासियों के दावे खारिज किये गए, उन्हें दावे खारिज होने का न कोई कारण बताया गया और न अपील का कोई अवसर दिया. केन्द्र सरकार की उदासीनता का आलम यह है कि उसने तो सुप्रीम कोर्ट में जरूरी तारीखों पर भी अपना वकील भेजना भी उचित नहीं समझा.
अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि 2005 से पहले से जंगलों में रह रही तमाम अनुसूचित जनजातियों के तमाम सदस्यों व तीन पीढियों से अधिक समय से वन में रह रहे अन्य निवासियों का उन वनों पर व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकार बनता है. सरकारी मशीनरी ने आदिवासियों, आदिम जातियों और वनों में निवास करने वाले अन्य समुदायों को दस्तावजों के फेर में फंसा दिया बिना इस बात पर गौर किये कि आदिवासियों में दस्तावेजीकरण की कोई परंपरा नहीं है. वहां सब कुछ मौखिक है. उनके पास उन जमीनों के कोई पट्टे नहीं हैं जहां वे दर्जनों पीढियों से रह रहे या खेती कर रहे हैं.
ज्यादातर आदिवासियों को तो दावा प्रस्तुतिकरण से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की जानकारी नहीं है. वे तो एक ही बात जानते हैं कि ये नदियां और पहाड़ उनके मां-पिता हैं जिनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी है. जैसा कि नियमगिरि में हुआ. वेदांता की साजिशों के खिलाफ बारह की बारह ग्राम सभाओं ने एक सुर में कह दिया कि हमें वेदांता नहीं, हमारा पिता नियमगिरि चाहिए. इसने वर्षों से हमारा पोषण किया है और हम इसे नष्ट नहीं होने देंगे. क्या जंगल और वन्यजीव रक्षा का दावा करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के पास ऐसा व्यापक दर्शन है?
चूँकि न्याय पर मौजूदा तीनों मसलों में सरकार की भूमिका से वंचित तबके संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने सामूहिक रूप से 5 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है. कई राजनीतिक दलों ने इस बंद को समर्थन देने की घोषणा की है. निश्चित तौर पर प्रथम दृष्टया ये मामले कानूनी हैं लेकिन इनका असर दूरगामी होने वाला है. केन्द्रीय सरकार को सामाजिक न्याय और समावेशी लोकतंत्र के हक में इस कठिन समय में देश के वंचितों के साथ खड़े होना चाहिए. इससे देश के वंचितों की लोकतंत्र में आस्था मजबूत होगी.
(लेखक गंगा सहाय मीणा आदिवासी चिंतक एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं)